महात्मा गांधी के विचारो को गांधीवाद कहा जाता है। गांधीवाद के सम्बन्ध मे
सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है तो निश्चित रूप से गांधीवाद
जैसी कोई वस्तु नही हे। क्योंकि गांधीजी ने राजनीति सम्बन्धी क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत नही
किया है और न किसी वाद का संस्थापन ही किया।
गांधी जी ने स्वयं कहा था। गांधीवाद नामक कोई वस्तु नही है और न मै अपने पीछे
कोई सम्प्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। मेरा यह दावा भी नही हैकि मैने किसी नये सिद्धांत का
अविष्कार किया है। मैने तो सिर्फ शाश्वत सत्यो को अपने नित्य जीवन से और प्रतिदिन के
प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास मात्र किया है।
गांधीजी के अनुयायियो ने गांधीजी के बिखरे अव्यवस्थित विचारो को संकलित कर क्रमबद्धता प्रदान कर गांधीवाद नाम दिया।
गांधीवाद की परिभाषा
1. पट्टमि सीता रमैया के अनुसार- ‘‘गांधीवाद कुछ नियमों एवं सिध्दांतो का संकलन मात्र न होकर जीवन का दर्शन है यह जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्राचीन भारतीय दर्शन के आधार पर तल करने का प्रयास करता है’’2. गांधीजी के प्रमुख विचार उनकी प्रमुख पुस्तक हिन्द स्वराज्य आत्मकथा (सत्य के साथ मेरे प्रयोग) सत्याग्रह सर्वोदय शान्ति और युद्ध मैं अहिंसा आदि में मिलते हे।
इसके अलावा साप्ताहिक पत्र दक्षिण अफ्रीका मैं इंडियन ओपिनियन भारत में हरिजन नवजीवन हरिजन सेवक आदि मे मिलते है।
गांधीवाद की विशेषताएं
1. गांधीजी के मतानुसार - ‘‘परमात्मा ही सत्य है शुध्द अन्तरात्मा की वाणी ही सत्य है। लोक सेवा ईश्वर प्राप्ति के साधन का आवश्यक अंग है। गांधीजी मानव समूह को भगवान का विराट रूप मानते थे और उनकी सेवा को भगवान की सेवा।’’2. एक व्यावहारिक दर्शन- गांधीवाद वास्तविकता पर आधारित है। गांधीजी कर्मयोगी थे। कर्म
मे विश्वास करते थे। उनका दर्शन उनके निजी अनुभवो सत्य के प्रयोगो आरै
अहिंसा पर आधारित है।
3. सत्याग्रह- गांधीवाद का मूल आधार सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य को
आरूढ़ करना। सत्याग्रह मे छलकपट धोखा का परित्याग कर प्रेम एवं सत्य
के नैतिक शास्त्र का प्रयोग करना पडता है। सत्याग्रह तो शक्तिशाली और
वीर मनुष्य का शस्त्र है।
4. अहिंसा पर आधारित- गांधीजी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक सुव्यवस्थित
स माज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति हो सकती है।
अहिंसा का अर्थ किसी भी रूप मे अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना
है। एवं अत्याचारी की इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना
भी है। अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है।
5. आदर्श राज्य की स्थापना- गांधीजी अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते
थे। जिसमे समस्त मानव सदगुणी एवं विवेकशील हो । उसमें स्वार्थमयी हितो
का कोई स्थान न हो। सभी सुखी संपन्न एव निश्चित जीवन यापन करेंगे।
6. सर्वोदय- गांधीजी सभी लोगो की उन्नति उदय एवं कल्याण मे विश्वास करते
थे। उनका विश्वास था कि उपेक्षित गरीबो के उत्थान से ही समाज एवं राष्ट्र
की प्रगति संभव है।
7. छूआछूत विरोधी- छूआछूत समाज का एक गम्भीर दोष रहा है। गांधीजी समाज में
व्याप्त छूआछूत को मिटाकर सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे
समाज में अछूतो के विकास एवं कल्याण के लिए उन्होने उनको ‘‘हरिजन’’
नाम दिया।
8. विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था तथा न्यासधारिता का सिध्दांत- गांधीवाद मे आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ न्यासधारिता के
सिध्दांत का भी उल्लेख किया गया है उनका विचार था कि पूंजीपतियो को
हृदय परिवर्तन द्वारा सम्पत्ति की न्यासी (ट्रस्टी) बना दिया जाय और
पूंजीपति उस सम्पत्ति का प्रयोग सम्पूर्ण समाज के हित के लिये करें।
9. साध्य तथा साधन- गांधीवाद पूर्णतया एक नैतिक दर्शन है। साध्य के साथ साथ साधन
भी नैतिक हो इस बात पर गांधीवाद में विशेष जोर दिया गया है। उनका मत
था कि यदि पवित्र साधन नही मिलते हो तो उस साध्य को ही छोड़ दो।
10. विश्व बन्धुत्व और अन्तर्राष्ट्रवाद का समर्थन- गांधीजी मानव कल्याण के समर्थक थे। वे समस्त मानव का हित
चिंतन करते थे। उनहोने सामा्रजयवाद का विरोध किया तथा विश्व शांति
तथा अन्तर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया।
गांधीवाद के प्रमुख सिद्धांत
गांधीवाद के प्रमुख सिद्धांत को सार रूप में शीर्षको के अन्तर्गत
प्रस्तुत किया जा सकता है-
1. सत्य और अहिंसा के विचार
गांधीवादी दर्शन मे सत्य एवं अहिंसा के विचारो को सर्वोच्च स्थान
प्राप्त है सत्य एवं अहिंसा मानव के धार्मिक भावो के विकास के लिये अनिवार्य
है गांधीजी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। हिंसा जीवन की पवित्रता तथा
एकता के विपरीत है।
2. साध्य तथा साधन की पवित्रता
गांधीजी का मत है कि साध्य पवित्र है तो उसे पा्रप्त करने का
साधन भी पवित्र होना चाहिए इसलिए गांधीजी ने साध्य (स्वतंत्रता) प्राप्त
करने के लिये पवित्र साधन (सत्य और अहिंसा) को अपनाया।
3. राजनीति और धर्म
गांधीजी राजनीति और धर्म में गहरा सम्बन्ध मानते थे। गांधीजी कहते
थे धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति तो मृत्यु जाल है
क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। वे कहते थे कि धर्म मानव जीवन के
प्रत्येक कार्य को नैतिकता का आधार प्रदान करता है।
4. सत्ता का विकेन्द्रीयकरण
गांधीजी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण
के पक्ष में थे-
- राजनीतिक शक्तियो का विकेन्द्रीयकरण-सत्ता के विकेन्द्रीयकरण से गांधीजी का अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायतो को अपने गांवो का प्रबंध और प्रशासन करने का सब अधिकार दे दिये जाने चाहिए ग्राम का शासन ग्राम पंचायत द्वारा संचालित हो और ग्राम पंचायत ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका हो।
- आर्थिक शक्तियो का विकेन्द्रीयकरण- गांधीजी आर्थिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में थे व े बडे़ उद्योगो के स्थान पर कुटीर उद्योगो की स्थापना का पक्ष लेते थे।
6. गांधीजी ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। गांधीजी के अनुसार
साम्राज्यवादी देश न केवल अधीन देश का आर्थिक नैतिक शोषण करता है
वरन विश्व युध्दो का कारण भी यही है। गांधीजी का मत था कि नि:शस्त्रीकरण
और अहिंसक विश्व समाज से साम्राज्यवाद का स्वयं अंत हो जायेगा।
गांधीवाद की आलोचना
गांधीवादी विचारधारा के सैध्दांितक दृष्टिकोण से यद्यपि सभी व्यक्ति सहमत है किन्तु उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनेक आधारो पर लागे असहमति व्यक्त करते हे। गांधीवाद की आलोचना के प्रमुख आधार है-
1. गांधीवाद काल्पनिक विचारधारा है - आलोचकों के द्वारा गांधीवादी दर्शन के विरूद्ध यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह वास्तविकता से दूर कोरा काल्पनिक व भावनात्मक दर्शन है। वर्तमान में परिस्थितियों में आदर्श राज्य व अहिंसात्मक राज्य की स्थापना करना वास्तविकता से परे है। क्योंकि पुलिस और सैन्य बल के अभाव में राज्य में न ता े शांति व्यवस्था रह सकती है और न ही वह राष्ट्र स्थायी रह सकता है।
2. गांधीवाद में मौलिकता का अभाव- आलोचकों ने गांधीवाद में मौलिकता का अभाव बता या हे। क्योंकि गांधीजी ने गीता बाइबिल आरै टालस्टाय आदि स े विचार उधार लिए है गांधीजी ने कोई नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नही किया है।
3. अहिंसा अव्यावहारिक- गांधीजी ने अहिंसा पर अत्यधिक बल देकर उसे आधुनिक समय में अव्यावहारिक बना दिया है। आलोचकों का मत है कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ का समाधान सदैव अहिंसा से करना असंभव है।
4. सत्याग्रह का सिध्दांत अव्यावहारिक- गांधीजी हर जगह सत्याग्रह के सिध्दातं को लागू करना चाहते है परंतु हर जगह सत्याग्रह सफल नही हो सकता। गांधीजी का यही अहिंसात्मक साधन आज हिंसात्मक व तोड़फोड़ का रूप लेता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु अनुचित साधना े को अपनाकर सत्यागह्र का दुरूपयोग कर रहे है।
5. विरोधाभासी दर्शन- गांधी दर्शन एक विरोधाभासी दशर्न है एक तरफ गांधीजी पूंजीवादी की बुराइर् करते है ता े दूसरी ओर न्यासधारिता की आड़ लेकर उसे बनाये रखना चाहते है।
6. औद्योगीकीकरण का विरोध- गांधीजी आर्थिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीयकरण का पक्ष लेत े हएु कुटीर उद्योगो का समर्थन किया है। आलोचको का मत है कि कुटीर उद्योगा े से भारत जैसे विस्तृत देश की जनसख्ं या की आवश्यकता की पूि तर् होना असंभव है।
4. सत्याग्रह का सिध्दांत अव्यावहारिक- गांधीजी हर जगह सत्याग्रह के सिध्दातं को लागू करना चाहते है परंतु हर जगह सत्याग्रह सफल नही हो सकता। गांधीजी का यही अहिंसात्मक साधन आज हिंसात्मक व तोड़फोड़ का रूप लेता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु अनुचित साधना े को अपनाकर सत्यागह्र का दुरूपयोग कर रहे है।
गांधीवाद तथा मार्क्सवाद में समानताएं
- मानवतावादी विचारधारा- गांधीवाद और माक्र्सवाद दोनो का ही उद्देश्य मानव का विकास और लोक कल्याण है।
- वर्गविहीन समाज की स्थापना - दोनो ही विचारधारा का अंतिम लक्ष्य वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है।
- श्रम की सर्वोपरिता - दोनो ही विचारधारा में श्रम को सभी के लिये अनिवार्य बताया गया है। सभी व्यक्ति परिश्रम करें और खायें कोई किसी का शोषण न करें।
- विश्व शांति के समर्थक - दोनो ही विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि विश्व युध्दो से मुक्त कोई भी शक्तिशाली देश कमजोर देश का शोषण न करें।
गांधीवाद तथा मार्क्सवाद में असमानताएं
- साधन व साध्य के सम्बन्ध मे अंतर - गांधीवाद में श्रेष्ठ साध्य के साथ साथ साधनो की पवित्रता को भी आवश्यक माना गया है जबकि माक्र्सवाद में पवित्र साध्य प्राप्ति के लिये साधनो की पवित्रता मे विश्वास नही करता।
- व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी अधिकार - गांधीवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी नही है जबकि माक्र्सवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है।
- वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर मतभेद- गांधीवाद में जहां वर्ग संघर्ष के लिये कोई स्थान नही है वहीं साम्यवाद (मार्क्सवाद) वर्ग संघर्ष को लक्ष्य प्राप्ति के लिये आवश्यक मानता हे।
- लोक तंत्र के सम्बन्ध में विश्वास - गांधीजी का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। उन्होने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये लोकतंत्रीय पध्दति को आवश्यक बताया है। किन्तु साम्यवाद (मार्क्सवाद) लोकतंत्र को निकम्मो का शासन कहकर उसकी निंदा करते है।
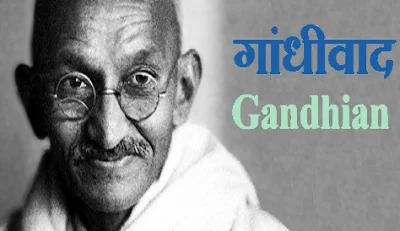
लोग कहते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया देश को आजाद जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कराया देश को आजाद कराया है सरदार वल्लभ भाई पटेल शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने गांधीजी चरखा चलाते थे लोग कहते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद करा था जो आदमी चलाता है बताइए आदमी देश को कैसे आजाद करा सकता है यदि हमारे सैनिकों को हाथों में एके-47 की जगह चरखा थमा देना चाहिए हमारे देश की भलीभांति रक्षा कर सकें इस तरह की सोच रखना भी गलत होगा क्योंकि यदि हमारे सैनिक भी गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में रहे तो हमारे देश का नामो निशान मिट जाएगा
ReplyDeleteवर्तमान में गांधी वादी "कश्ती" जर्जर ही सही पर लहरों से टकराती तो हैं
Deleteबिना माली के बाग टिक नहीं पाता है
DeleteDost tum itne hi gyani ho to Gandhi ko kyu padh.rahe ho. Or govt me baithe log itne pagal h ki Gandhi ki pic indian currency me laga diya. Bhai jis bhi history ki book padho achhe se padho
DeleteSocial media ka gyan yaha mat pelo
Padhai kr lete to syd aaj Gandhi ji ke bare me galat nhi bolte
DeleteSahi bat h
ReplyDeleteYaa i'm agree....
ReplyDeleteभारत को आजाद गाँधी जी ने नहींं कराया है भारत को तो आजाद और भी महान पुरुषो ने भी कराया है ज़ैसे डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जी ने सुभाषचंद्र बोस ने ,भगत सिंह ने , राज गुरु ने आदि और भी महान लोगों ने भारत को आजाद कराया है
ReplyDeleteCaret देश को केवल गाँधी जी ने ही नहीं बल्कि और भी महान क्रांतिकारीयों ने भी कराया है ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि गाँधीजी आहिंसा वादी थे और ऐसा बीलकुल भी नहीं हुआ की बीना लड़ाई के देश आजाद हुआ अनेक देश वासियों ने अपने परण और पाता नहीं क्या क्य खोना पड़ा है इसलिए ऐसा कहा न बिल्कुल गलत है मैं तो कहती हूँ कि ऐसा गाना भी गलत है दे दी हमे आजादी बीना खणक बीना डाल क्यों कि बीना लड़ाई आजादी नहीं मिली जय हिंद
ReplyDeleteJyada bahas mat Karo bro
DeleteGandhi ji ko nation of bapu kaha jaata hain
Ghandhi ji ne jo kiya wo sai kiya taa wo bhi desh ko ajadh krwana hee chahte te bs unka Tarika kuch alg taa agar wo koi kam acche nhi krte to duniya aaj unhe yaad nhi karti
ReplyDeleteJai Hind Jai Bharat 🇮🇳🇮🇳
I think agar gandhi ji ke bhroshe baithe hote to desh ho gya tha phir aajad......... Shanti se aur pyar se hi agr angrejo ko jana hota to humare itne sahid nhi hote......... Bhai ankhein kholo
DeleteGandhi bs ek popular hasti tha uski sachai kisi ko nhi pta ......sadar patel,br Ambedkar,etc inki vjh se asli azadi milli h hamein or gandhi ne toh adha desh hamara un pakistaniyo ko de diya ..
ReplyDelete