वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति' : 'Globalization' अंग्रेजी का शब्द है । इस शब्द की रचना, इस प्रकार होती है : मूल शब्द Globe' है, इसका अर्थ है गोल अथवा पृथ्वी | Globe काAdjective (विशेषण) Globalहोता है। जिसका अर्थ है Taking in the whole world ( पूरे विश्व को समाहित करने वाला) Globalसे बना हुआ Verb (क्रिया) Globalize है | Globalize Verb (क्रिया) को Noun (संज्ञा) के रूप में परिवर्तित करने पर इस प्रक्रिया को व्यक्त करने वाला शब्द Globlization है, जिसका अर्थ Process of taking in the whole world (पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया ) है । अंग्रेजी शब्द Globalization का हिन्दी अनुवाद 'वैश्वीकरण' है। इसका पर्यायवाची शब्द भूमण्डलीकरण है।
चेंबर शब्दकोश के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्वव्यापी बना देना या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना ।
रंगराजन के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ है सूचनाओं, विचारों, तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, वित्त और लोगों का देश की सीमाओं से बाहर प्रवाह के द्वारा समाजों एवं अर्थव्यवस्था का एकीकरण ।
स्टीपन गिल के अनुसार, वैश्वीकरण पूंजी एवं वस्तुओं की सीमा से पार गतिशीलता की कारोबार लागत
की कमी है । जिसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों एवं वस्तुओं को शामिल किया गया है ।
वैश्वीकरण की परिभाषा
मॅलकोल्म वेटर्स के अनुसार, वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें भूगोल द्वारासामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को दबाया जाता है, जिससे लोग इस बात के लिये जागरूक होने लगते हैं कि उनका प्रश्चप्रवण हो रहा हैं।
आर. रॉबर्ट्सन' के अनुसार, वैश्वीकरण प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए वे मानते हैं कि वैश्वीकरण लादने का दबाव तेजी से बढ़ा हैं, किन्तु, इसने अन्तरात्मक शक्ति प्रदान किया। राबर्ट्सन ने वैश्वीकरण को एक ऐसी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया हैं जो दुनिया के दबाव और दुनिया की चेतना के तीव्रीकरण दोनों से संयुक्त रूप से सम्बन्धित है।
रवि प्रकाश पाण्डेय के अनुसार, वैश्वीकरण, अन्तर्वेशन और बहिष्करण की एक जटिल प्रक्रिया है । इसमें विश्व बाजार, विभिन्न आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति आदि के एकीकरण का अन्तर्वेशन हो रहा है, जबकि राष्ट्र-राज्य की प्रभुसत्ता और स्वदेशीयता आदि का बहिष्करण हो रहा हैं ।
रंगराजन के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ है सूचनाओं, विचारों, तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, वित्त और लोगों का देश की सीमाओं से बाहर प्रवाह के द्वारा समाजों एवं अर्थव्यवस्था का एकीकरण ।
स्टीपन गिल के अनुसार, वैश्वीकरण पूंजी एवं वस्तुओं की सीमा से पार गतिशीलता की कारोबार लागत
की कमी है । जिसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों एवं वस्तुओं को शामिल किया गया है ।
वैश्वीकरण का इतिहास
भूमंडलीकरण सामान्यतः एक ऐसी अवधारणा होनी चाहिए थी कि पूरे विश्व में एक संस्कृति विकसित हो जो पूरे भूमंडल को एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर सारी दुनिया के मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होती । इस रूप में यह हमारी वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा के अनुकूल होता जिसमें विश्व मानवता के कल्याण की शिव कामना है किंतु आज वर्तमान रूप में वैश्विकरण एक ऐसी धारण है जिसका मूलाधार बाजार, बाजारवाद और उपभोक्तावाद है। पूरी दुनिया को अपने बाजार के रूप में परिवर्तित कर विश्व की सर्वोच्च– सुपर शक्ति अमेरिका अपने रूप में ढालकर सांस्कृतिक दृष्टि से अपना बनाने, आर्थिक दृष्टि से अपने न्यस्त स्वार्थों की संपूर्ति केलिए पूरे विश्व को एक रंग में रँगने के संकल्प को कार्य रूप दे चुका है, पूरा विश्व उसके द्वारा परिकल्पित मॉल संस्कृति बनकर रह गया है।
यह वैश्विकरण एक प्रकार से पूरी दुनिया का अमेरिकीकरण है जो सारे राष्ट्रों की स्थानिक संस्कृति, जातिय चेतना को पूरी तरह लील कर अपने रंग में रंग डालने की बड़ी भारी सफल कूटनीति है जिसके कारण पूरा विश्व उसकी चपेट में आ चुका है। एक प्रभंजन के प्रवेग से अमेरिकी अर्थनीतियों और तथाकथित भूमंडलीय सांस्कृति, सांस्कृति की चारों ओर अपना पसारा पसारा चुकी है। यह चाहिए था कि पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों की सभ्यताएँ –संस्कृतियाँ मिलकर मानव कल्याण के एक मंगलकारी स्वप्न को यथार्थ रूप में देने का प्रयत्न करती किंतु हुआ इसके बिलकुल उलट कि प्रत्येक देश की संस्कृति के शुभ और शिव को अमेरिकी संस्कति के दानवी डैनों ने दबोच कर एक न-अंकल सैम–संस्कृति का पसारा चहुँ ओर फैला दिया। प्रत्येक राष्ट्र के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई कि वह पुरातन को न छोड़ पाने के मोह में रहते हुए भी इस नयी संस्कृति के कम्बल को ओढ़ने लगा, पूरी तरह अपने से चिपकाये हुए, उसमें एक नई ऊष्मा खोजने लगा। इसलिए न-न करते हुए भी सभी उससे चिपट कर पूरी सरी गले लगाने में ही अगाध प्रसन्नता अनुभव करने लगे। सूचना प्रौध्योगिकी, तकनीकी उन्नती, उपग्रत दृ सैटेलाइट–क्रांति ने राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं का अर्थ समाप्त कर पूरी दुनिया को एकमेल करने का बीड़ा उठा लिया है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय अस्मिता, भाषा संस्कार, बोलियाँ, भाषाएँ, लोक - संस्कृति, सब कुछ मटियोमेट, होकर अमेरिकीकरण की प्रक्रिया में है। भारतीय संस्कृति का चरित्र प्रारंभ से ही उदार रूप में सर्वसमावेशी रहा है, जितनी भी संस्कृतियों के कारवाँ यहाँ आए, वे यही की संस्कृति में घुलमिल कर एकमेल हो गए।
किंतु अब उत्तर आधुनिक समय में वैश्वीकरण की यह आँधी जितने प्रवेश से भारत में आई, हमारी संस्कृति के भी पैर उखाड़ दिए हैं, अपने पैरों को पूरी शक्ति से रोपे रखने के सभी प्रयत्न प्रायः निष्फल होते नजर आ रहे हैं, हम भी वैश्विकरण के बहाव में बहकर नव विकास के नाम पर इसी वैश्विक गाँव- ग्लोबल गाँव - का अंग बनते जा रहे हैं। “परिवेश ने हमारे ऊपर इन स्थितियों को पूरी तरह थोपकर हमें उपभोक्तावादी संसार के ऐसे मायावी व्यूह में डाल दिया है कि हम उससे निकल पाने की जुगत नहीं निकाल पा रहे हैं। पूरी दुनिया ऐसी उपभोक्तावादी संस्कृति में तब्दील हो रही है जहाँ पैसा ही सब कुछ हैं ।
वैश्वीकृत नव उदारवाद ने गरीबी और युवा बेरोजगारी की दर पूरे विश्व में किस प्रकार बढ़ायी है इसे अब अमेरिका से उठे जनांदोलन - बॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो, आक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसे बवंडर के रूप में ले लिया। यह संकेतित करता है कि वैश्वीकरण, ने विश्व के गरीबों- जो अमेरिका में अपने को हम 99 प्रतिशत हैं- वी आर नाइनटी–नाइन परसेंट कह रहे हैं— को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी - दुनिया में कमोबेश यही स्थितियाँ भूमंडलीकरण की सौगात के रूप में सामने आ रही हैं। बाजारवाद के युग में साहित्य और कलाओं की कोई उपयोगिता सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं दे रही है, किंतु वैश्वीकरण के इस घोर तमस में भी कलाएँ और साहित्य ही मनुष्य की संस्कृति के श्रेष्ठ को बचाने का उपक्रम कर सकती हैं। यह सुखप्रद स्थिति है कि सभी कलाएँ और साहित्य भूमंडलीकरण की दानवी शक्तियों का भरपूर विरोध कर रही हैं।
वैश्वीकरण एक आधुनिक सिद्धांत नहीं है। सदियों से पहले वैश्वीकरण की अवधारण हुई थी। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी शब्द Globalisation का पर्यायवाची शब्द है | Global शब्द ही परिवर्तन का सूचक है। सन् 1960 में इसका प्रयोग दुनिया से सम्बन्धित या पूरे संसार के अर्थ में किया था। मार्शल माक्लुहान (Marshall Mucluhan) 1964 इसका प्रयोग विश्व ग्राम के लिए किया था। सूचना और संचार माध्यमों के आविष्कार के पहले ही उन्होंने संसार भर को एक रस्सी में पिरोने की कामना की थी ।
आफ्रिकी लोगों के उपनिवेश से वैश्वीकरण की शुरूआत मान सकते हैं। दूसरी तरफ से कहें तो 5 वीं और 6 वीं सदी के सौराष्ट्रसम और बुद्धिम नामक दो धर्म के द्वारा इसका आविर्भाव हुआ । सन् 1776 में प्रकाशित एडम स्मित की पुस्तक "वेलथ ऑफ नेशन” में पूँजीवादी व्यवस्था एवं स्वतंत्र व्यापार के बारे में बाताया है। प्रस्तुत रचना के अनुसार वैश्वीकरण का आरंभ 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जा सकता है। अट्लान्टिक महासमुद्र को पार करनेवाला प्रथम तार सन् 1866 में आया। इस सदी के अन्त तक आते- आते संसार तार (Tele phone), वैश्विक बाजार (Global Commodity Market), वैश्विक ब्रान्ट नाम (Global brand name), वैश्विक संघ (Global association), सामाजिक आन्दोलन (Social movement), नारीवादी क्रियाकलाप (Feminist activation) आदि के द्वारा वैश्विक संबंध बढ़ गये। 19 वीं सदी के अंत में इन सबकी प्रगती कोलनीय सत्ताधारियों की उन्नती का भी कारण बना। वैश्वीकरण में बहुत अधिक प्रगति पिछली आधी सदी में हुई। जेट हवाई जहाज, उपग्रह, दूरदर्शन आदि का प्रयोग बहुत बढ़ गया। आजकल समाज सबसे अधिक वैश्विक हो रहा है।
वैश्वीकरण की विशेषताएं
- मुक्त व्यापार की बाधाएँ दूर करना ।
- आर्थिक वैश्वीकरण, व्यापार, निवेश और लोगों के प्रवास द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण ।
- यह सूचनाओं, विचारों, तकनीकी, वस्तुओं तथा लोगों का देश की सीमाओं से बाहर प्रवाह के द्वारा समाज तथा व्यवस्थाओं का एकीकरण है ।
- वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं और सामग्री का लोगों के हित के लिए मुक्त विनिमय है ।
- यह अंतर्राष्ट्रीय के पार लोगों और ज्ञान की गतिशीलता है ।
वैश्वीकरण क्यों?
वैश्वीकरण के समान इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह विश्व के सभी लोगों के लिए विकास प्राप्त कर सकता है, तथा उन्हें लगातार कायम रहने वाले विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता कर सकता है। महासचिव कोफी अन्नान ने अपने भाषण के शीर्षक - “हम दुनिया के लोग : 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका” में कहा कि वैश्वीकरण के लाभ स्पष्ट हैं - अघिक तेज गति से विकास, रहन-सहन का उच्चतर स्तर, देशों और व्यक्तियों के लिए नए-नए अवसर। इसके लिए हमें इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। श्रम मानदण्ड न्यायोचित होने चाहिए, मानवाधिकारों का आदर किया जाना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व अर्थव्यवस्था की कई रुकावटें दूर कर दी हैं। इससे व्यापार में खुलापन आया है और विदेशी निवेश के प्रति उदारता में वृद्धि हुई है। इसके कारण वित्तीय व व्यापार क्षेत्र में उदार नीतियों का निर्माण किया गया है। आज जेट विमान, उपग्रह, इंटरनेट की वजह से देशकाल की सीमाएं अर्थहीन हो गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उदारीकरण हो गया है। राष्ट्रीय सम्प्रभुताएं सीमाविहीन होने लगी हैं। दुनिया सिकुड़कर एक 'Global Village' बन गई है। इसने विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए हैं। आज विश्व व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय निगमों का ही कब्जा हो गया है।
1970-90 के दौरान विश्व के सकल घरेलू उत्पादन में विश्व व्यापार की भागेदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई
है। 1980-1996 के दौरान प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित
क्षेत्र का भी विकास हुआ है। विदेशी मुद्रा बाजार का विकास चौंकाने वाला है।
1983 में प्रतिदिन विदेशी मुद्रा बाजार का
विकास चौंकाने वाला है। 1983 में प्रतिदिन विदेशी मुद्रा बाजार में 60 अरब डॉलर का लेन देन होता था जो 1996 में 1200
अरब डॉलर तक पहुंच गया।
इस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण सम्प्रभुता, स्वायत्तता और स्वतन्त्रता की संकीर्ण परिभाषाएं सिकुड़ गई हैं। संचार क्रांति और वैश्वीकरण ने जातीयता को गतिशील बना दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे के काफी पास आ गया है। भौगोलिक दूरियां समाप्त हो गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध नए रूप में पेश हुए हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति व देश को आर्थिक विकास में भागेदारी के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसलिए अधिक तेज आर्थिक विकास तथा विकास के नए अवसर प्रत्येक को प्रदान करने के लिए भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण बहुत अधिक जरूरी है।
वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क
यद्यपि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व के देशों को कुछ लाभ भी पहुंचाया है, लेकिन उसने लोगों को नकारात्मक रूप में अधिक प्रभावित किया है। इसके लाभ न्यायोचित व समान नहीं हैं। विश्व बाजार अब तक सहभागी सामाजिक लक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-- वैश्वीकरण कमजोर देशों के लिए हानिकारक है। पार-सीमा व्यापार तथा निवेश कमजोर देशों के आर्थिक हित में नहीं है। यह इन देशों में लोकतन्त्रीय नियंत्रण को शिथिल कर देता है। इसमें आर्थिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्धों पर भारी पड़ते हैं। इसमें मुक्त व्यापार तथा सुरक्षावाद के बीच टकराव पैदा हो जाता है।
- वैश्वीकरण विकसित देशों के हितों का पोषक है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विकसित देशों के हितों के संवर्द्धन में ही कार्य करती है। इसके कारण उत्पादकता तथा निवेश दरें काफी गिरी हैं। बढ़े हुए वित्तीय प्रवाह ने पूंजी बाजारों में अधिक तरलता तथा वास्तविक ब्याज दरों को काफी ऊँचा किया है। इससे शेयरों की खरीद तथा सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रक्रिया ने विकसित देशों को ही ज्यादा लाभ पहुंचाया है, विकासशील देशों को नहीं।
- इसने विकसित और विकासशील देशों के बीच आय की असमानता को बढ़ा दिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कम वेतन पर ही अच्छा कारोबार करके विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाया है। 1960 में यह अन्तर 30.1 का था, जो अब 82.1 का हो गया है। इसी कारण विकासशील देश पूंजी पलायन का सहन करके भी विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
- इसने विकासशील देशों पर ऋणों के भार को बढ़ा दिया है और इससे विश्व में वित्तीय संकट आने की संभावना बढ़ गई है।
- वैश्वीकरण का संस्थागत ढांचा भी भेदभावपूर्ण है। इसमें एक तरफ तो व्यापार तथा पूंजी प्रवाह को मुक्त आधार प्रदान किया गया है और दूसरी तरफ तकनीक तथा श्रम प्रवाह को रोका जा रहा है। विकसित देशों की तो यह इच्छा है कि विकासशील देश अपने बाजारों को उनके लिए खोल दें लेकिन तकनीकी हस्तांतरण की मांग न करें।
- यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सम्प्रभुता का हनन करती है। विश्व व्यापार संगठन के दायरे में राष्ट्रीय सम्प्रभुता के विषय भी आ गए हैं। वैश्वीकरण किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिवधियों और सामाजिक सम्बन्धों को भी प्रभावित करने में सक्षम हैं।
- इससे स्थानीय व्यापारिक हितों को अधिक हानि हो रही है। इसने स्थानीय व्यापारिक निगमों को बहुराष्ट्रीय निगमों का पिछलग्गू बना दिया है।
- यह नव-उपनिवेशवाद को मजबूत बना रहा है। मौजूदा विश्व आर्थिक संस्थाएं विकसित देशों को लाभ पहुंचा रही हैं और विकासशील देशों का शोषण कर रही हैं।
इन कमियों के बावजूद भी यह कहा जा सकता है। कि इस प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे संबंधित आर्थिक संस्थाओं की भूमिका के महत्व को बढ़ा दिया है। इसमें अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इसको समाप्त करने की नहीं है, बल्कि आवश्यकता इसके संकीर्ण लक्ष्यों को समाप्त करने की है। इसके लिए मुक्त व्यापार नीतियों को दबाव मुक्त बनाया जाना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अत्यधिक सहयोग देना चाहिए। वर्तमान विश्व आर्थिक संस्थाओं की कुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए।
आज WTO
के विश्वव्यापी खतरों से निपटने के लिए काफी सहयोगी की आवश्यकता है। इसलिए इसके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक
दुष्प्रभावों को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं समृद्धि की प्रक्रिया के रूप में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इससे
वैश्वीकरण के लाभ विकासशील देशों को भी मिलने लगेंगे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक नए युग की शुरुआत होगी।
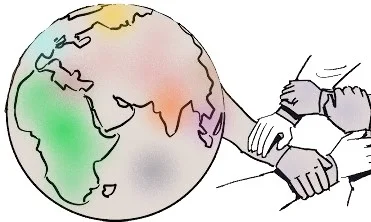
ही
ReplyDeleteContent always be selected and perfect to topic at this site.And language is simple and behavioural.To understand the topic is easy.
ReplyDelete