भारतेन्दु
की कविताओं के विषय विविध हैं। भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश,
प्रकृति आदि विभिन्न संदर्भों पर आधारित इनकी कविताओं में एक ओर प्राचीन काव्य परंपरा
का पालन किया गया है तो दूसरी ओर नवीन चेतना और आधुनिक काव्यधारा का प्रवर्तन
हुआ है। राजभक्ति, देशभक्ति, दास्यभाव और माधुर्य भाव आदि के चित्रण भी मिलते हैं।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन परिचय
भारतेन्दु हरिशचंद्र का जन्म ९ सितंबर १८५० को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था । उनके पिता भी अच्छे कवि थे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के
पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरिधरदास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पांच वर्ष की अवस्था अर्थात्
बाल्यकाल में काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया था। पांच वर्ष की आयु में मां का स्वर्गवास हो गया, 10 वर्ष की अवस्था में पिता
का।
भारतेन्दु का मूल नाम हरिश्चन्द्र है। अल्पायु में ही हरिश्चन्द्र ने कवित्व प्रतिभा एवं सर्वतोमुखी रचना क्षमता का ऐसा
परिचय दिया कि तत्कालीन साहित्यकारों तथा पत्रकारों ने सन् 1880 ई. में उन्हें भारतेन्दु की उपाधि प्रदान कर सम्मानित
किया। भारतेंदु, कवि, साहित्यकार, पत्रकार सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि वचन सुधा तथा हरिश्चन्द्र चंद्रिका
भारतेंदु के संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का भाषा और साहित्य दोनों पर अत्यधिक गहन प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य भाषा को परिमार्जित करके उसे अति मधुर, चलता एवं स्वच्छ स्वरूप प्रदान किया है उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाषा को संस्कारित किया है। भारतेंदु को वर्तमान गद्य का प्रवर्तक माना गया। भाषा का शिष्ट सामान्य निखरा हुआ रूप भारतेंदु की कला ने उपस्थित किया। पुराने पड़े हुए शब्दों का स्थानांतरण करके काव्य भाषा में भी वे चलतापन एवं सफाई लाने में सफल हुए हैं।
साहित्य को नवीन मार्ग पर लाकर उसे शिक्षित जनता का सहचर बनाया। भारतेंदु ने पुराने रास्ते पर पड़े हुए साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जन-जन के साथ जोड़ दिया। जनता एवं साहित्य के बीच बढ़ती हुई खाईं को उन्होंने पाट दिया। साहित्य को नवीन प्रवृत्ति एवं नई दिशा देने का श्रेय भारतेन्दु को है। हरिश्चन्द्र की भाषा को हरिश्चन्द्री हिंदी नाम दिया गया। इसके आविर्भाव के साथ नए-नए लेखक तैयार होने लगे।
भारतेन्दु ने दो शैलियों को व्यवÎहृत किया है - भावावेश की शैली तथा तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश में उनकी भाषा में वाक्य प्राय: लघुतर होते जाते हैं तथा पदावली सरल आम बोल-चाल की होती है जिसमें बहु प्रचलित आम बोल चाल में प्रयोग में आने वाले अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश कभी कभी हो जाता है।
जहां चित्त के किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है तथा चिंतन हेतु अवकाश मिलते ही उनकी भाषा में साधुता एवं गंभीरता आने के साथ साथ वाक्यों का आयाम विस्तृत होने लगता है किन्तु अन्वय में जटिलता नहीं आने पाती है।
तथ्य निरूपण अथवा वस्तु वर्णन के अवसर पर उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली प्रधान हो जाती है किन्तु इसे भारतेन्दु की वास्तविक भाषा नहीं कहा जा सकता। उनकी वास्तविक भाषा संस्कृतनिष्ठ नहीं थी। भाषा चाहे जैसी हो उनके वाक्यों के अन्वय में जटिलता को स्थान न मिलकर सरलता विद्यमान थी। वाग्वैदंग्ध्य या चमत्कार के स्थान पर उनके भावों में हृदय स्पर्शिता एवं धार्मिकता विद्यमान है।
साहित्य में नाटक, निबंध आदि की रचना द्वारा उन्होंने
खड़ी बोली की गद्य शैली के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी कविताएं विविध-विषय-विभूषित हैं जिनमें
भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश तथा प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर उन्होंने विपुल परिमाण में काव्य रचना
की।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाएं
भारतेंदु ने काव्य, नाटक, स्त्री शिक्षा तथा इतिहास आदि पर लेखनी उठाई। भारतेंदु ग्रंथावली उनके समग्र साहित्य का संकलन
है।
1. काव्य - प्रेम मालिका, सतसई श्रृंगार, भारत वीणा, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय
प्रेम-पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, विजयिनी-विजय-वैजयंती आदि प्रमुख काव्य
रचनाएं हैं।
2. नाटक - नील देवी, भारत जननी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, चन्द्रावली नाटिका, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, सती प्रताप,
दुर्लभ बंधु एवं अंधेर नगरी आदि नाट्य कृतियां हैं। अन्य पुस्तक काल चक्र है।
3. स्त्री शिक्षा - बालाबोधिनी।
4. संपादन - कवि वचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन, हरिश्चन्द्र चंद्रिका।
5. इतिहास - काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, दिल्ली दरबार दर्पण, महाराष्ट्र देश का इतिहास।
6. अनूदित - बंगला से हिंदी अनुवाद - विद्या सुंदर नाटक मुद्राराक्षस, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय।
7. निबंध - सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चन्द्र, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चन्द्र।।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की साहित्यिक विशेषताएं
इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपनी अनेक रचनाओं में जहां वे प्राचीन प्रवृत्तियों का अनुगमन करते रहे हैं वहीं नवीन काव्य
धारा के प्रवर्तन का श्रेय भी इन्हीं को है। राजभक्त होते हुए भी देश भक्त हैं, दास्य भक्ति के साथ साथ माधुर्य भक्ति का निर्वाह
किया है। एक ओर उन्होंने नायक-नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उनके लिए नए कर्तव्य क्षेत्र भी
निर्देशित किए हैं। शैली इतिवृत्तात्मक होते हुए हास्य-व्यंग्य का तीखा प्रहार करने वाली भी है। अभिव्यंजना क्षेत्र में भी उन्होंने
परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों को स्वीकारा है। यह उनकी प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति का प्रमाण है। प्रबल हिंदीवादी होते
हुए भी उन्होंने उर्दू शैली को कविता के लिए चुना है। काव्य भाषा हेतु ब्रजभाषा को अपनाया है किन्तु खड़ी बोली में दशरथ
विलाप तथा फूलों का गुच्छा की रचना की है।
काव्य रूपों की विविधता उनकी अनन्य विशेषता है। छंदोबद्धता का निर्वाह
करते हुए भी गेय पद शैली को अपनाया है। भारतेंदु काव्य क्षेत्र के नवयुग में वे अग्रदूत थे। अपनी ओजस्विता, सरलता,
भाव-व्यंजना, एवं प्रभ विष्णुता में उनका काव्य इतना सशक्त एवं प्राणवान हो गया है कि तत्कालीन सभी कवियों को
अत्यधिक प्रभावित किया है।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का भाषा और साहित्य दोनों पर अत्यधिक गहन प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य भाषा को परिमार्जित करके उसे अति मधुर, चलता एवं स्वच्छ स्वरूप प्रदान किया है उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाषा को संस्कारित किया है। भारतेंदु को वर्तमान गद्य का प्रवर्तक माना गया। भाषा का शिष्ट सामान्य निखरा हुआ रूप भारतेंदु की कला ने उपस्थित किया। पुराने पड़े हुए शब्दों का स्थानांतरण करके काव्य भाषा में भी वे चलतापन एवं सफाई लाने में सफल हुए हैं।
साहित्य को नवीन मार्ग पर लाकर उसे शिक्षित जनता का सहचर बनाया। भारतेंदु ने पुराने रास्ते पर पड़े हुए साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जन-जन के साथ जोड़ दिया। जनता एवं साहित्य के बीच बढ़ती हुई खाईं को उन्होंने पाट दिया। साहित्य को नवीन प्रवृत्ति एवं नई दिशा देने का श्रेय भारतेन्दु को है। हरिश्चन्द्र की भाषा को हरिश्चन्द्री हिंदी नाम दिया गया। इसके आविर्भाव के साथ नए-नए लेखक तैयार होने लगे।
भारतेन्दु ने दो शैलियों को व्यवÎहृत किया है - भावावेश की शैली तथा तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश में उनकी भाषा में वाक्य प्राय: लघुतर होते जाते हैं तथा पदावली सरल आम बोल-चाल की होती है जिसमें बहु प्रचलित आम बोल चाल में प्रयोग में आने वाले अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश कभी कभी हो जाता है।
जहां चित्त के किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है तथा चिंतन हेतु अवकाश मिलते ही उनकी भाषा में साधुता एवं गंभीरता आने के साथ साथ वाक्यों का आयाम विस्तृत होने लगता है किन्तु अन्वय में जटिलता नहीं आने पाती है।
तथ्य निरूपण अथवा वस्तु वर्णन के अवसर पर उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली प्रधान हो जाती है किन्तु इसे भारतेन्दु की वास्तविक भाषा नहीं कहा जा सकता। उनकी वास्तविक भाषा संस्कृतनिष्ठ नहीं थी। भाषा चाहे जैसी हो उनके वाक्यों के अन्वय में जटिलता को स्थान न मिलकर सरलता विद्यमान थी। वाग्वैदंग्ध्य या चमत्कार के स्थान पर उनके भावों में हृदय स्पर्शिता एवं धार्मिकता विद्यमान है।
Tags:
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
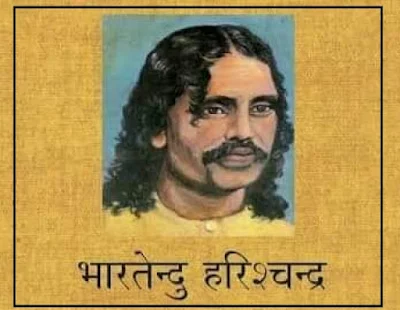
Bahut badiya content hai
ReplyDelete